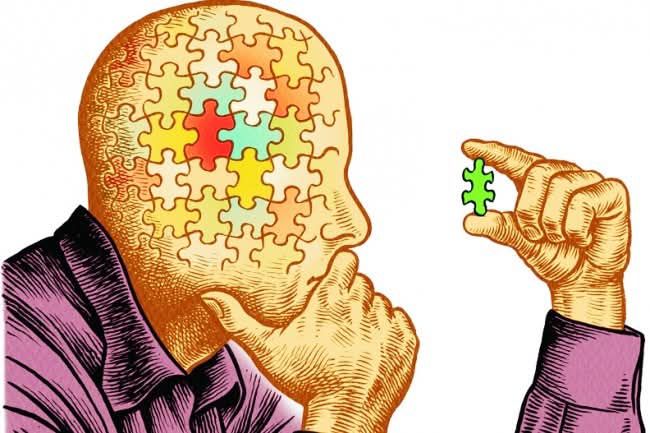
सुदेश आर्या
एक व्यक्ति बरसों की मेहनत के बाद लकड़ी का एक खूबसूरत फ़्रेम तैयार करता है। शानदार नक्काशी और चमकदार फ़्रेम। अब वो इस फ्रेम को लेकर बाज़ार में निकलता है कि इसमें लगाने लायक मनभावन इतनी ही खूबसूरत कलाकृति भी मिल जाए।
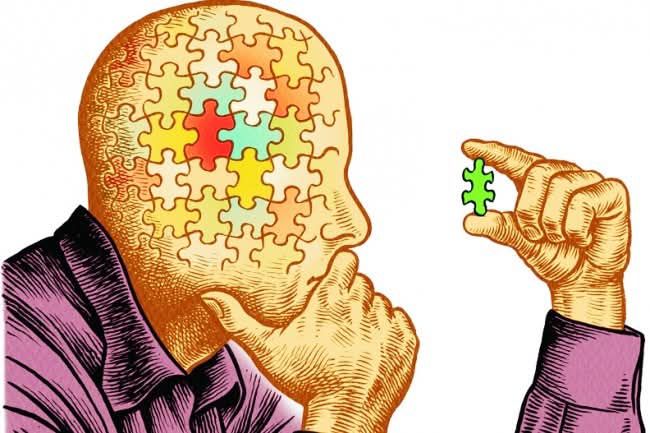
पैसों की कहीं कोई कमी नहीं है। महंगी से महंगी कलाकृति वो खरीद सकता है, लेकिन मुसीबत ये है कि “जीवनरूपी” फ़्रेम के आकार की उतनी ही खूबसूरत कलाकृति उसे नहीं मिल पाती। कोई आकार से लम्बी है तो कोई चौड़ी। फ़्रेम कितना भी खूबसूरत हो, उसमें अगर कलाकृति ना हो तो वो अधूरा ही लगेगा। ये फ़्रेम भी अधूरा ही रह जाता है।
बुद्धिमान लोग उसे समझाते भी हैं कि भाई तुझे पहले कलाकृति लेनी चाहिए थी, फ़्रेम तो उसके हिसाब से ऊपर-नीचे हो जाता। लेकिन वो आदमी भी क्या करे, अब तो फ़्रेम बन चुका है।
पर क्या फ्रेम तोड़ना इतना आसान है जिसे बनाने में बरसों लगे हैं। लेकिन हमें ऐसे फ्रेम तोड़ने ही पड़ेंगे। नास्तिकों को भी, आस्तिकों को भी। वैज्ञानिकों को भी, धार्मिकों को भी। तर्कवादियों को भी और भाववादियों को भी।
कलाकृति को हासिल करने के लिए पूर्वनिर्मित फ्रेम तोड़ना ही होगा। जैसे कट्टर धार्मिक होना कंडीशंड है, वैसे ही कट्टर नास्तिक होना भी कंडीशंड है। ना ही अति तार्किक और ना ही अति कट्टर। अतिरेक तो नुकसान ही करता है।




